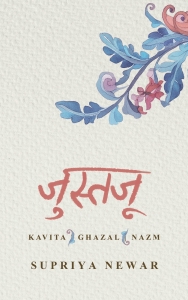
नज़्म – सोमवार
आज खिड़की पर
गुड़गुड़ाते कबूतरों को दाने दिए
और फिर सुर्ख़ियों के आगे
अखबार के पन्नों को
आखिर तक पलटते हुए
इत्मीनान से टटोला
फिर यूँ हुआ
की माँ का फ़ोन आया
और ये न कह कर
कि मैं एक मीटिंग में हूँ
पुछा उससे मैंने
के था उसके दिल में क्या समाया
यूँ तो अख्तरी बाई से
परिचय है मेरा एक अरसे का
पर इन दिनों
तफ्सील से उन्हें सुनने का
मौका ही न बन पढ़ा
उनकी आवाज़ ने दुहरायी एक भूली दास्तान
एक गुज़रा ज़माना फिर हुआ बयान
उधर मासी ने खिचड़ी थी पकाई
जिसको पापड़ और हरी चटनी के साथ मैंने खायी
एक नरम सी धूप
अब कमरे में आने लगी थी
और खिचड़ी के बाद
उबासी सताने लगी थी
छोटे से बरामदे में
जब मैंने दरी बिछाई
तो न जाने कहाँ से
मुई रज़ाई
खुद ब खुद
खींची आयी
पता न चला
कब हाथों से किताब
गोद में फिसल गयी
पता न चला
कब लोरी सुनाके
जाड़े कि धुप से
आँख लग गयी
शाम हुयी तो दूर से
शंख की आवाज़ आयी
शाम हुयी तो इंस्टेंट नहीं
ताज़ा घोटी हुयी कॉफी
मैंने चढ़ाई
बिन बुलाये एक पुराना दोस्त चला आया
खूब बातें की उसने
मैंने भी खूब
सुर में सुर लगाया
दिन ढलने के बाद
एक चराग़ आज जलाया
और खिले हुए सुर्ख फूलों को
गुलदान में सजाया
महके हुए इस आलम में
कलम जो मैंने उठायी
तो एहसास हुआ
की एक सदी के बाद
मैंने दफ्तर की घंटी
सोमवार को नहीं थी बजायी
About the Author
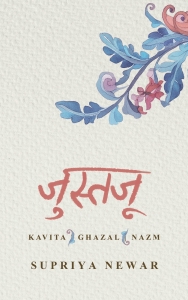



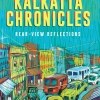
Comments